Please click here to read this in English
टैरिफ, आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें, और वैश्विक व्यापार की शक्ति का खेल
अंतरराष्ट्रीय संबंधों की जटिल दुनिया में, हमेशा अरबों डॉलर के रक्षा सौदे या उच्च-तकनीकी सहयोग ही सबसे अधिक विवाद का कारण नहीं बनते। कभी-कभी, यह मकई जैसी सामान्य चीज भी हो सकती है। महीनों से, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक सुलगता व्यापार विवाद गरमाने की कगार पर है, और इसके केंद्र में एक ही persistent अमेरिकी मांग है: “1.4 अरब लोग हमारा मक्का क्यों नहीं खरीदेंगे?” यह सवाल, जिसे हाल ही में अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक सहित अमेरिकी अधिकारियों ने उठाया है, दोनों वैश्विक दिग्गजों के बीच कृषि और भू-राजनीतिक तनाव के मूल में जाता है।
अमेरिकी दबाव: 1.4 अरब का बाजार
संयुक्त राज्य अमेरिका, दुनिया का निर्विवाद मक्का उत्पादन और निर्यात का राजा, अपनी सुनहरी फसल के लिए नए बाजार खोजने के मिशन पर है। 2025-26 के लिए 75 मिलियन टन के अनुमानित निर्यात के साथ, अमेरिका के पास बेचने के लिए एक बड़ा अधिशेष है। इस तात्कालिकता को चीन से मांग में नाटकीय गिरावट से और बल मिला है, जो कभी इसका शीर्ष खरीदार था। 2022 में, चीन ने 5.21 बिलियन डॉलर का अमेरिकी मक्का आयात किया था। 2024 तक, यह संख्या घटकर मात्र 331 मिलियन डॉलर रह गई, जिससे अमेरिकी किसान एक अनिश्चित स्थिति में आ गए हैं।
इस आर्थिक दबाव का सामना करते हुए, वाशिंगटन ने भारत पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं, एक ऐसा देश जिसकी आबादी बहुत बड़ी और बढ़ती हुई है। अमेरिकी अधिकारियों ने खुले तौर पर अपनी निराशा व्यक्त की है, व्यापार संबंधों को “एकतरफा सड़क” के रूप में वर्णित किया है जहां भारत अपना सामान अमेरिका को बेचता है जबकि अपने बाजारों, विशेष रूप से कृषि, को मजबूती से बंद रखता है। तर्क सरल है: इतनी बड़ी आबादी के साथ, भारत अमेरिकी मक्के की थोड़ी मात्रा भी क्यों नहीं खरीद रहा है?
भारत का प्रतिरोध: एक बहु-स्तरीय रक्षा
अमेरिकी मक्के के लिए अपने दरवाजे खोलने से भारत का इनकार केवल संरक्षणवाद का एक सरल कार्य नहीं है। यह एक सावधानीपूर्वक विचार की गई नीति है जो तीन मुख्य स्तंभों पर बनी है:
- किसानों के एक राष्ट्र की रक्षा करना: भारत मक्का में काफी हद तक आत्मनिर्भर है, जो अपनी खपत के लगभग बराबर उत्पादन करता है – सालाना लगभग 42 मिलियन टन। इस क्षेत्र में छोटे किसानों का वर्चस्व है जो मूल्य झटकों के प्रति अत्यंत संवेदनशील हैं। अमेरिकी मक्का काफी सस्ता होने (भारत के थोक मूल्य ₹22-23/किग्रा की तुलना में ₹15/किग्रा से कम) के कारण, सस्ते आयात की बाढ़ लाखों भारतीय किसानों की आजीविका को नष्ट कर सकती है।
- महान जीएमओ दीवार: यह शायद सबसे महत्वपूर्ण बाधा है। अमेरिका में उगाए जाने वाले 90% से अधिक मक्का आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) है, जिसे कीटों और शाकनाशियों का विरोध करने के लिए इंजीनियर किया गया है। दूसरी ओर, भारत में जीएम खाद्य फसलों पर सख्त प्रतिबंध है, जिसमें एकमात्र अपवाद गैर-खाद्य जीएम कपास है। यह प्रतिबंध जैव सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर जीएम उत्पादों के संभावित दीर्घकालिक प्रभाव के बारे में गहरी चिंताओं पर आधारित है।
- उच्च टैरिफ: गैर-जीएम मक्के के लिए भी, भारत में एक कड़ी टैरिफ संरचना है। यह 15% शुल्क पर सीमित मात्रा में आयात (0.5 मिलियन टन तक) की अनुमति देता है, लेकिन उससे अधिक की किसी भी मात्रा पर 50% का भारी शुल्क लगता है। यह नीति बड़े पैमाने पर आयात को हतोत्साहित करने और घरेलू बाजार की रक्षा करने के लिए बनाई गई है।
आगे का रास्ता: क्या कोई समझौता होगा?
गतिरोध के बावजूद, दोनों देश फिर से बातचीत की मेज पर हैं। भारतीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की वाशिंगटन यात्रा सहित हालिया उच्च-स्तरीय वार्ता को “सकारात्मक और दूरंदेशी” बताया गया है। एक संभावित समझौता जो सामने आया है वह भारत के लिए विशेष रूप से इथेनॉल उत्पादन के लिए अमेरिकी मक्का आयात करने का एक प्रस्ताव है। चूंकि यह मक्का खाद्य श्रृंखला में प्रवेश नहीं करेगा, इसलिए यह जीएम भोजन के संवेदनशील मुद्दे को दरकिनार करते हुए भारत की जैव ईंधन जरूरतों को पूरा करने का एक तरीका हो सकता है।
हालांकि, समाधान की राह चुनौतियों से भरी है। भारत को एक शक्तिशाली सहयोगी के साथ अपने व्यापार संबंधों का प्रबंधन करने के साथ-साथ अपनी विशाल कृषक आबादी के हितों की रक्षा करने के नाजुक संतुलन का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर, अमेरिका पर अपने किसानों, एक प्रमुख राजनीतिक निर्वाचन क्षेत्र, के लिए प्रदर्शन करने का दबाव है, खासकर एक चुनावी वर्ष में।
सामाजिक संदेश
भारत-अमेरिका मक्का विवाद एक व्यापारिक विवाद से कहीं बढ़कर है; यह उन विभिन्न प्राथमिकताओं का प्रतिबिंब है जो राष्ट्रों को आकार देती हैं। जबकि एक पक्ष मुक्त बाजारों और वैश्विक व्यापार का समर्थन करता है, दूसरा आत्मनिर्भरता और अपने सबसे कमजोर नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी परस्पर जुड़ी हुई दुनिया में, हर नीतिगत निर्णय, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न लगे, के दूरगामी परिणाम होते हैं। सच्ची साझेदारी और प्रगति किसी पर अपनी इच्छा थोपने में नहीं, बल्कि एक ऐसा मध्य मार्ग खोजने में निहित है जो सभी की अनूठी जरूरतों और मूल्यों का सम्मान करता है।


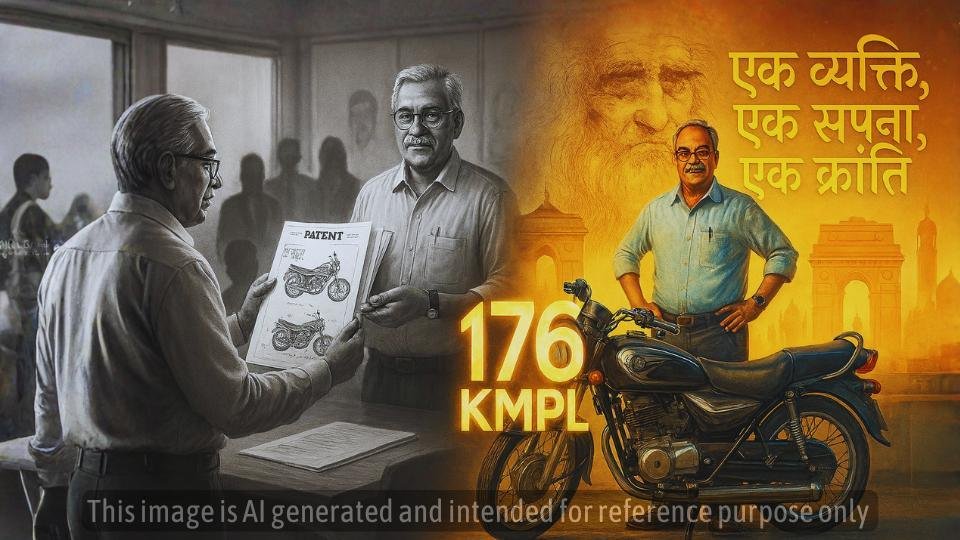

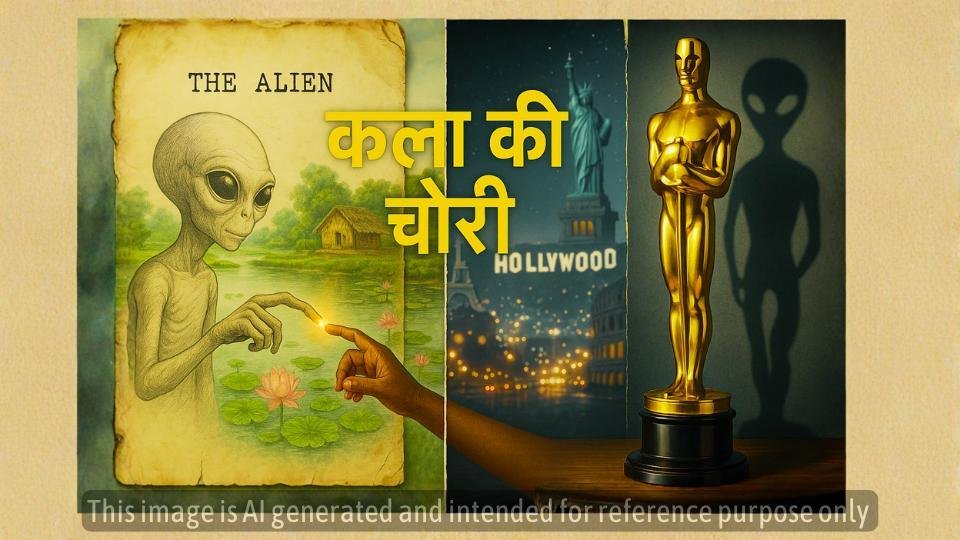


Leave a Reply