Please click here to read this in English
भारत ने चरम गरीबी को ऐतिहासिक रूप से कम करने में सफलता पाई है, जहाँ वित्तीय वर्ष 2022–23 में चरम गरीबी दर घटकर 2.3 प्रतिशत रह गई, जो कि 2011–12 में 16.2 प्रतिशत थी। इस दौरान लगभग 17.1 करोड़ लोगों को अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त $2.15 प्रतिदिन (PPP) चरम गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया। यह उल्लेखनीय प्रगति सतत आर्थिक विकास, लक्षित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे कि मनरेगा, वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों और ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार के चलते संभव हुई। फिर भी, क्षेत्रीय असमानताओं, कल्याणकारी योजनाओं में कभी-कभार होने वाली गड़बड़ियों और ग़रीबी के गैर-आर्थिक पहलुओं जैसी चुनौतियाँ अब भी बनी हुई हैं।
ताज़ा आंकड़े
- 2011–12 से 2022–23 के बीच, भारत की चरम गरीबी दर (प्रति दिन $2.15 से कम आय पर जीवनयापन करने वाले) 16.2 प्रतिशत से घटकर 2.3 प्रतिशत हो गई, जिससे लगभग 17.1 करोड़ लोग चरम गरीबी से बाहर आए।
- ग्रामीण चरम गरीबी 18.4 प्रतिशत से घटकर 2.8 प्रतिशत हो गई, जबकि शहरी चरम गरीबी 10.7 प्रतिशत से घटकर 1.1 प्रतिशत पर आ गई, जिससे ग्रामीण-शहरी अंतर 7.7 प्रतिशत अंक से घटकर 1.7 प्रतिशत अंक रह गया।
- निम्न-मध्यम आय वाले देशों के लिए निर्धारित $3.65 प्रतिदिन गरीबी रेखा के अनुसार, गरीबी दर 61.8 प्रतिशत से घटकर 28.1 प्रतिशत हो गई, जिससे 37.8 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया।
- विश्व बैंक की “पावर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ: अप्रैल 2025”, जो अध्यक्ष अजय बंगा के नेतृत्व में जारी की गई, इस बात को रेखांकित करती है कि रोजगार वृद्धि ने कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या वृद्धि को पीछे छोड़ दिया है।
ऐतिहासिक संदर्भ और पृष्ठभूमि
- 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत ने औपनिवेशिक भू-राजस्व प्रणालियों से उपजे व्यापक ग्रामीण अभाव को विरासत में पाया, जिसने भूमि स्वामित्व को कुछ हाथों में केंद्रित कर दिया था और खाद्य सुरक्षा की बजाय नकदी फसलों को प्राथमिकता दी थी।
- 1990 के दशक तक, $1.90 प्रतिदिन (PPP) आय मापदंड पर गरीबी 40 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या को प्रभावित कर रही थी; सरकार ने कई ग्रामीण रोजगार और राहत कार्यक्रमों जैसे कि जवाहर रोजगार योजना (1989), रोजगार आश्वासन योजना (1993), और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (2001) का प्रयोग किया।
- 2005 में मनरेगा अधिनियमित किया गया, जिसने प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 100 दिन के वेतनयुक्त रोजगार की गारंटी दी — यह दुनिया का सबसे बड़ा सार्वजनिक कार्य कार्यक्रम बना और सामाजिक सुरक्षा में अधिकार-आधारित दृष्टिकोण का आरंभ हुआ।
प्रगति को गति देने वाली सरकारी योजनाएँ
- मनरेगा: इस ऐतिहासिक अधिनियम ने चरम मौसम में ग्रामीण परिवारों के एक चौथाई से अधिक के लिए सुरक्षा जाल प्रदान किया और करोड़ों कार्य-दिनों का सृजन कर ग्रामीण आय और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा दिया।
- प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY): 2014 में शुरू हुई इस योजना ने 45 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले, जिससे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण संभव हुआ और लीकेज (भ्रष्टाचार) में कमी आई।
- स्वास्थ्य और पोषण: आयुष्मान भारत जैसी योजनाएँ और मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का विस्तार स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच और स्कूल में उपस्थिति में सुधार कर गरीबी उन्मूलन को परोक्ष रूप से समर्थन दे रहे हैं।
- राज्य स्तरीय पहलें: केरल की “चरम गरीबी उन्मूलन परियोजना” और आंध्र प्रदेश की “जगन्नन्ना विद्या दीवेना” जैसे आक्रामक राज्य प्रयास गैर-आर्थिक गरीबी आयामों को लक्षित कर रहे हैं।
ज़मीन से आई कहानियाँ
- उत्तर प्रदेश के एक ग्रामीण क्षेत्र में, छोटी किसान मीना देवी ने मनरेगा की मजदूरी का उपयोग गाँव के जलाशय की मरम्मत के लिए किया, जिससे कृषि उत्पादकता दोगुनी हो गई और उनके बच्चों को प्रतिदिन 40 किमी पानी लाने के लिए पैदल चलने से मुक्ति मिली।
- झारखंड में, मछली बेचने वाले से शिक्षक बने बिश्वनाथ नारू ने स्लम बच्चों के लिए एक मुफ्त स्कूल चलाया, यह दर्शाते हुए कि कैसे सामुदायिक नेतृत्व सरकारी योजनाओं के पूरक के रूप में कार्य कर सकता है।
- तमिलनाडु में, शांति भवन स्कूल की पूर्व छात्रा काव्या मुस्कुराते हुए याद करती हैं कि कैसे मध्याह्न भोजन ने उन्हें स्कूल में बनाए रखा, और कॉलेज तक पहुँचने का मार्ग प्रशस्त किया — यह एक छोटी सफलता है जो लाखों अन्य यात्राओं की गूंज है।
चुनौतियाँ और आगे का रास्ता
- गड़बड़ी और गबन: सामाजिक ऑडिट से पता चला है कि चार वर्षों में मनरेगा के तहत लगभग ₹935 करोड़ की गड़बड़ी हुई, जिसमें से केवल 1.34 प्रतिशत राशि ही वसूल की जा सकी।
- असमानता: उपभोग असमानता में गिरावट के बावजूद, आय असमानता बढ़ी है, जो अधिक समावेशी विकास नीतियों की आवश्यकता को उजागर करती है।
- गैर-आर्थिक गरीबी: स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर को कवर करने वाली बहुआयामी गरीबी अब भी 15.5 प्रतिशत है, जो बताती है कि आय से परे कई कठिनाइयाँ बनी हुई हैं।
- बुनियादी ढांचे की कमी: ग्रामीण सड़कों, बिजली और स्वच्छता की कमी पूर्ण सशक्तिकरण में बाधा डालती है, जिसके लिए नए सिरे से निवेश की आवश्यकता है।
निष्कर्ष
भारत की चरम गरीबी दर को 2.3 प्रतिशत तक घटाना एक ऐसा मील का पत्थर है जिसे समन्वित नीतिगत कार्रवाई, आर्थिक विकास और जमीनी स्तर की लचीलापन के बल पर प्राप्त किया गया है। इन उपलब्धियों को बनाए रखने और आगे बढ़ाने के लिए, भारत को गड़बड़ियों पर लगाम लगानी होगी, गैर-आय गरीबी आयामों को मजबूत करना होगा, और क्षेत्रीय और सामाजिक समावेशी विकास सुनिश्चित करना होगा।



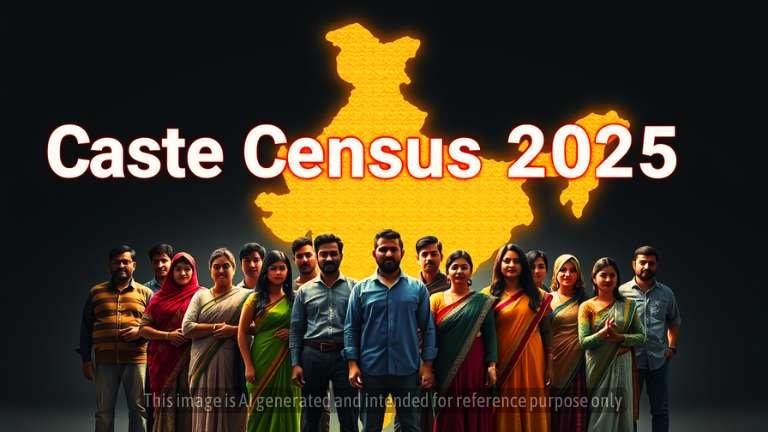


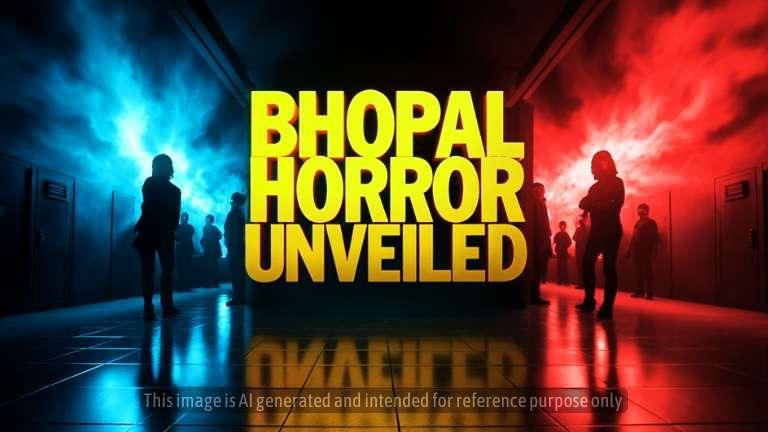
Leave a Reply